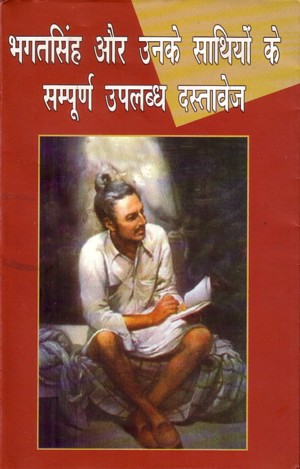हिन्दी के भविष्य के बारे में चिन्ता भरी चर्चा हो रही हो, तो हम यह सवाल भी पूछ सकते हैं कि दुनिया की अन्य भाषाओं में भी क्या आज ऐसी ही चर्चाएँ हो रही हैं? और अगर हाँ तो वे क्या सोच रहे हैं, कर रहे हैं और उनसे क्या हम कुछ सीख सकते हैं. चूँकी मैं इटली में रहता हूँ, यूरोप में फ्राँसिसी, जर्मन आदि भाषाओं की इस तरह की चर्चा सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस समय मैं केवल इतालवी भाषा में होने वाली चर्चा की करना चाहता हूँ.
इस वर्ष इटली के एक हो कर राष्ट्र बनने की 150वीं वर्षगाँठ मनायी जा रही है. इस बात पर इतने झगड़े हो रहे हैं कि सुन कर अचरज होता है. अचरज इसलिए कि बहस में लोग इटली की एकता के विरुद्ध टीवी और अखबारों में खुले आम बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई "देशद्रोही" कह कर या "देश का अपमान किया" कह कर, कोई यह बात नहीं कर रहा कि इन्हें जेल होनी चाहिये या इन पर मुकदमा होना चाहिये. जैसे कि उत्तर पूर्वी इटली के राज्य आल्तो अदिजे (Alto Adige) के मेयर ने टीवी पर साफ़ कह दिया कि वह इटली की एकता के किसी समारोह में भाग नहीं लेंगे और न ही उन्हें इटली की एकता की कोई खुशी है. इसका कारण है कि इटली का यह हिस्सा प्रथम विश्वयुद्ध के पहले आस्ट्रिया का हिस्सा था और युद्ध में आस्ट्रिया की हार के बाद इटली से जोड़ दिया गया था. आज भी वहाँ के बहुत से लोग आपस में और घर में जर्मन भाषा बोलते हैं. हालाँकि यूरोपीय संघ बनने के बाद से इटली और आस्ट्रिया के बीच की सीमा का आज सामान्य जीवन में कुछ असर नहीं, पर पुराने घाव हैं जिन्हें वह खुले आम कहते हैं.
इटली की सरकार में "लेगा नोर्द" (Lega Nord) नाम की पार्टी भी है जिसके लोग सोचते हैं कि उत्तरी इटली के लोग, दक्षिणी इटली से भिन्न और ऊँचे स्तर के हैं. इनका पुराना नारा था कि "रोम के लोग सब चोर हैं और हम चोरों की सरकार को नहीं मानेगें". इस नारे को उन्होंने सरकार में शामिल होने के बाद, कुछ सालों के लिए स्थगित कर दिया है. यह पार्टी उत्तरी इटली को अलग देश बनाने की बात करती थी, पर सरकार में आने के बाद इनका राग थोड़ा सा बदल गया है. अब यह लोग अलग देश बनाने की बजाय बात करते हैं राज्यों के फेडरेलाइज़ेशन की, यानि देश के विभिन्न राज्यों को अपने निर्णय लेने की और अपनी नीतियाँ निर्धारित करने की स्वतंत्रता हो. देश की एकता की 150वीं वर्षगाँठ को इनमें से कुछ लोग शोक दिवस के रूप में देखते हैं, इसलिए इनमें से बहुत से लोग इस बात से भी सहमत नहीं कि इस वर्ष राष्ट्र एकता दिवस की 17 मार्च को विषेश राष्ट्रीय छुट्टी दी जाये.
"सारे देश में एक दिन की छुट्टी नहीं की जा सकती. उससे तो हमारी फैक्टरियों का, हमारे काम का बहुत नुक्सान होगा. वैसे ही मन्दी चल रही है, उस पर से एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी, यह हम नहीं मान सकते", इस तरह की बातें करने वाले स्वयं सरकारी मंत्री भी थे. पहले सरकार ने घोषणा की कि 17 मार्च को पूरे देश में सरकारी छुट्टी होगी, पर जब सरकारी मंत्री ही इस छुट्टी के खिलाफ़ बोलने लगे तो सरकार ने कहा कि इस विषय पर मंत्री मीटिंग में बात की जायेगी. एक महीने तक बहस होती रही कि यह छुट्टी दी जाये या नहीं. आखिरकार छुट्टी को मान लिया गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कोई इस दिन अपनी फैक्ट्री, दुकान या सुपरमार्किट खोले रखना चाहता है तो उन्हें इसकी छूट होगी.
इस पर कुछ अन्य पार्टियों ने और कामगार यूनियनों ने अभियान चलाया कि देश की एकता के विरुद्ध बोलने वालों को करारा जवाब दिया जाये और कई दिनों से कह रहे हैं कि 17 मार्च को हर घर की एक खिड़की पर इटली का राष्ट्रीय झँडा लगा होना चाहिये. मेरी एक मित्र बोली, "यह दुनिया इतनी बदल गयी है कि समझ में नहीं आता कि हमारी पहचान क्या है? मैं पुरानी कम्यूनिस्ट हूँ, हम लोग राष्ट्रवाद के विरुद्ध लड़ते थे, हम कहते थे केवल अपने देश की बात नहीं, बल्कि दुनिया में शाँति होनी चाहिये. तब राष्ट्रीय झँडा वह दकियानूसी लोग लगाते थे जो कहते थे कि हमारा देश सब अन्य देशों से ऊँचा है, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, विदेशियों को देश से निकालो. आज वे दकियानूसी लोग देश का झँडा नहीं लगाना चाहते, और हम कम्यूनिस्ट हो कर देश का झँडा लगाने की बात रहे हैं."
इन चर्चाओं को सुन कर मुझे भारत में होने वाली कश्मीर या नागालैंड में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाये या नहीं वाली चर्चाएँ याद आती हैं, हालाँकि भारत में इस तरह की बातों पर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मरने मारने की बातें करने लगते हैं.
इस तरह की बहसों के साथ साथ, देश की भाषा के बारे में कुछ इस तरह की चर्चाएँ भी हो रही हैं जिसमे मुझे लगा कि शायद भारत में हिन्दी के बारे में होने वाली चर्चा से कुछ समानताएँ हैं.
इटली में हर क्षेत्र की अपनी स्थानीय बोली थी, लेकिन स्कूलों में केवल इतालवी भाषा में ही पढ़ायी होती है. पिछले कुछ सालों में वह लोग बढ़े हैं जो "हमें अपनी स्थानीय बोलियों पर गर्व है" की बात करते हैं. यह लोग इन स्थानीय भाषाओं में रेडियो प्रोग्राम करते हैं, नाटक, गीत समारोह आदि का आयोजन करते हैं, ब्लाग लिखते हैं. लेकिन युवा वर्ग को पुरानी स्थानीय बोलियों का उतना ज्ञान नहीं. धीरे धीरे स्थानीय बोलियाँ लुप्त हो रही हैं, युवा लोग घर में, और आपस में केवल इतालवी भाषा ही बोलते हैं.
दूसरी ओर पिछले दो दशकों में इटली में अंग्रेज़ी जानने बोलने की क्षमता पर भी बहुत सी बहसें हो रही हैं. नौकरी खोज रहे हों तो अंग्रेज़ी जानने से नौकरी मिलना अधिक आसान है. लेकिन भारत में हिन्दी की स्थिति से एक महत्वपूर्ण अंतर है. भारत में अच्छी नौकरी के लिए हिन्दी न भी आती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि यहाँ पर बिना अच्छी इतालवी भाषा जाने काम नहीं चल सकता. अब यहाँ अंग्रेज़ी पहली कक्षा से ही पढ़ायी जा रही है. कम्पयूटरों और तकनीकी विकास के साथ, इतालवी भाषा में अंगरेज़ी के शब्दों के आने से भी चिन्ता व्यक्त की जाती है कि हमारी भाषा बिगड़ रही है, इसका क्या होगा!
वामपंथी पार्टी के अखबार ल'उनिता (L'Unità) यानि "एकता" ने कुछ दिन पहले एक इतालवी चिट्ठाकारों की गोष्ठी आयोजित की जिसमें देश की एकता की बात की गयी कि देश का चिट्ठाजगत इस विषय में क्या सोचता है? एक जाने माने चिट्ठाकार लियोनार्दो (Leonardo) ने इस बारे में अपने चिट्ठे में लिखाः
तकनीकी में, विज्ञान में, इतिहास और कला में, आज कहीं भी विश्वविद्यालय स्तर की शोध का काम अगर हिन्दी में किया जाये तो उसे वह सम्मान नहीं मिलता जो अंग्रेज़ी में किये जाने वाले काम को मिलता है. शायद इसलिए कि आज उस 90 प्रतिशत की आर्थिक ताकत कम है. लेकिन कल तकनीकी के विकास के साथ जब वह 90 प्रतिशत इन विषयों को समझना जानना चाहेगा, तो हिन्दी में यह काम बढ़ेगा, इसलिए नहीं कि कुछ लोग हिन्दी प्रेमी हैं, बल्कि इसलिए कि बाज़ार उसकी माँग कर रहा है.

जिन्हें हम भारत में "अंग्रेज़ी भाषी" कहते हैं, उनमें से बहुत सा हिस्सा बोलने लायक अंग्रेज़ी तो जानता है पर वह भारतीय अंग्रेज़ी है जिसे समझने के लिए विदेशियों को अनुवाद की आवश्यकता होती है. इस अध कच्ची अंग्रेज़ी का विकास किस ओर होगा? शुद्ध अंग्रेज़ी की ओर या अपनी भाषाओं की ओर? जब भारतीय भाषाओं का बाज़ार बढ़ेगा तो क्या यह भारतीय अंग्रेज़ी एक दिन उन्हीं में घुल मिल जायेगी?
इस वर्ष इटली के एक हो कर राष्ट्र बनने की 150वीं वर्षगाँठ मनायी जा रही है. इस बात पर इतने झगड़े हो रहे हैं कि सुन कर अचरज होता है. अचरज इसलिए कि बहस में लोग इटली की एकता के विरुद्ध टीवी और अखबारों में खुले आम बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई "देशद्रोही" कह कर या "देश का अपमान किया" कह कर, कोई यह बात नहीं कर रहा कि इन्हें जेल होनी चाहिये या इन पर मुकदमा होना चाहिये. जैसे कि उत्तर पूर्वी इटली के राज्य आल्तो अदिजे (Alto Adige) के मेयर ने टीवी पर साफ़ कह दिया कि वह इटली की एकता के किसी समारोह में भाग नहीं लेंगे और न ही उन्हें इटली की एकता की कोई खुशी है. इसका कारण है कि इटली का यह हिस्सा प्रथम विश्वयुद्ध के पहले आस्ट्रिया का हिस्सा था और युद्ध में आस्ट्रिया की हार के बाद इटली से जोड़ दिया गया था. आज भी वहाँ के बहुत से लोग आपस में और घर में जर्मन भाषा बोलते हैं. हालाँकि यूरोपीय संघ बनने के बाद से इटली और आस्ट्रिया के बीच की सीमा का आज सामान्य जीवन में कुछ असर नहीं, पर पुराने घाव हैं जिन्हें वह खुले आम कहते हैं.
इटली की सरकार में "लेगा नोर्द" (Lega Nord) नाम की पार्टी भी है जिसके लोग सोचते हैं कि उत्तरी इटली के लोग, दक्षिणी इटली से भिन्न और ऊँचे स्तर के हैं. इनका पुराना नारा था कि "रोम के लोग सब चोर हैं और हम चोरों की सरकार को नहीं मानेगें". इस नारे को उन्होंने सरकार में शामिल होने के बाद, कुछ सालों के लिए स्थगित कर दिया है. यह पार्टी उत्तरी इटली को अलग देश बनाने की बात करती थी, पर सरकार में आने के बाद इनका राग थोड़ा सा बदल गया है. अब यह लोग अलग देश बनाने की बजाय बात करते हैं राज्यों के फेडरेलाइज़ेशन की, यानि देश के विभिन्न राज्यों को अपने निर्णय लेने की और अपनी नीतियाँ निर्धारित करने की स्वतंत्रता हो. देश की एकता की 150वीं वर्षगाँठ को इनमें से कुछ लोग शोक दिवस के रूप में देखते हैं, इसलिए इनमें से बहुत से लोग इस बात से भी सहमत नहीं कि इस वर्ष राष्ट्र एकता दिवस की 17 मार्च को विषेश राष्ट्रीय छुट्टी दी जाये.
"सारे देश में एक दिन की छुट्टी नहीं की जा सकती. उससे तो हमारी फैक्टरियों का, हमारे काम का बहुत नुक्सान होगा. वैसे ही मन्दी चल रही है, उस पर से एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी, यह हम नहीं मान सकते", इस तरह की बातें करने वाले स्वयं सरकारी मंत्री भी थे. पहले सरकार ने घोषणा की कि 17 मार्च को पूरे देश में सरकारी छुट्टी होगी, पर जब सरकारी मंत्री ही इस छुट्टी के खिलाफ़ बोलने लगे तो सरकार ने कहा कि इस विषय पर मंत्री मीटिंग में बात की जायेगी. एक महीने तक बहस होती रही कि यह छुट्टी दी जाये या नहीं. आखिरकार छुट्टी को मान लिया गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कोई इस दिन अपनी फैक्ट्री, दुकान या सुपरमार्किट खोले रखना चाहता है तो उन्हें इसकी छूट होगी.
इस पर कुछ अन्य पार्टियों ने और कामगार यूनियनों ने अभियान चलाया कि देश की एकता के विरुद्ध बोलने वालों को करारा जवाब दिया जाये और कई दिनों से कह रहे हैं कि 17 मार्च को हर घर की एक खिड़की पर इटली का राष्ट्रीय झँडा लगा होना चाहिये. मेरी एक मित्र बोली, "यह दुनिया इतनी बदल गयी है कि समझ में नहीं आता कि हमारी पहचान क्या है? मैं पुरानी कम्यूनिस्ट हूँ, हम लोग राष्ट्रवाद के विरुद्ध लड़ते थे, हम कहते थे केवल अपने देश की बात नहीं, बल्कि दुनिया में शाँति होनी चाहिये. तब राष्ट्रीय झँडा वह दकियानूसी लोग लगाते थे जो कहते थे कि हमारा देश सब अन्य देशों से ऊँचा है, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, विदेशियों को देश से निकालो. आज वे दकियानूसी लोग देश का झँडा नहीं लगाना चाहते, और हम कम्यूनिस्ट हो कर देश का झँडा लगाने की बात रहे हैं."
इन चर्चाओं को सुन कर मुझे भारत में होने वाली कश्मीर या नागालैंड में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाये या नहीं वाली चर्चाएँ याद आती हैं, हालाँकि भारत में इस तरह की बातों पर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मरने मारने की बातें करने लगते हैं.
इस तरह की बहसों के साथ साथ, देश की भाषा के बारे में कुछ इस तरह की चर्चाएँ भी हो रही हैं जिसमे मुझे लगा कि शायद भारत में हिन्दी के बारे में होने वाली चर्चा से कुछ समानताएँ हैं.
इटली में हर क्षेत्र की अपनी स्थानीय बोली थी, लेकिन स्कूलों में केवल इतालवी भाषा में ही पढ़ायी होती है. पिछले कुछ सालों में वह लोग बढ़े हैं जो "हमें अपनी स्थानीय बोलियों पर गर्व है" की बात करते हैं. यह लोग इन स्थानीय भाषाओं में रेडियो प्रोग्राम करते हैं, नाटक, गीत समारोह आदि का आयोजन करते हैं, ब्लाग लिखते हैं. लेकिन युवा वर्ग को पुरानी स्थानीय बोलियों का उतना ज्ञान नहीं. धीरे धीरे स्थानीय बोलियाँ लुप्त हो रही हैं, युवा लोग घर में, और आपस में केवल इतालवी भाषा ही बोलते हैं.
दूसरी ओर पिछले दो दशकों में इटली में अंग्रेज़ी जानने बोलने की क्षमता पर भी बहुत सी बहसें हो रही हैं. नौकरी खोज रहे हों तो अंग्रेज़ी जानने से नौकरी मिलना अधिक आसान है. लेकिन भारत में हिन्दी की स्थिति से एक महत्वपूर्ण अंतर है. भारत में अच्छी नौकरी के लिए हिन्दी न भी आती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि यहाँ पर बिना अच्छी इतालवी भाषा जाने काम नहीं चल सकता. अब यहाँ अंग्रेज़ी पहली कक्षा से ही पढ़ायी जा रही है. कम्पयूटरों और तकनीकी विकास के साथ, इतालवी भाषा में अंगरेज़ी के शब्दों के आने से भी चिन्ता व्यक्त की जाती है कि हमारी भाषा बिगड़ रही है, इसका क्या होगा!
वामपंथी पार्टी के अखबार ल'उनिता (L'Unità) यानि "एकता" ने कुछ दिन पहले एक इतालवी चिट्ठाकारों की गोष्ठी आयोजित की जिसमें देश की एकता की बात की गयी कि देश का चिट्ठाजगत इस विषय में क्या सोचता है? एक जाने माने चिट्ठाकार लियोनार्दो (Leonardo) ने इस बारे में अपने चिट्ठे में लिखाः
"आज जितने लोग इतालवी भाषा में लिखते हैं, छापते हैं, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. भाषा विषेशज्ञ रोना रोते हैं कि भाषा का स्तर खराब हो रहा है, और उनकी बात अपनी जगह पर ठीक भी है. लेकिन मात्रा की दृष्टि से देखा जाये तो इतालवी भाषा में पिछले एक वर्ष में इतना लिखा गया जितना इंटरनेट के आविष्कार के बाद के पहले पंद्रह सालों में नहीं लिखा गया था. आज इंटरनेट पर इतालवी भाषा के चिट्ठे, वेबपन्ने, चेट, नेटवर्क फ़ल फ़ूल रहे हैं, हर कोई लिखना चाहता है.क्या इसका मतलब है कि भारत में इंटरनेट के फ़ैलने से हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ने का मौका मिलेगा? भारत में धीरे धीरे इंटरनेट का विस्तार हो रहा है, साथ ही हिन्दी, तमिल, तेलगू, मराठी, बँगाली आदि भाषाओं में लिखने का विस्तार भी हो रहा है. नयीं तकनीकें जो भारत में बन रही है, टेलीफ़ोन, कम्पयूटर, ईपेड आदि, इन सबको केवल पैसे वालों के लिए ही नहीं बल्कि जनता के बाज़ार में बिकना है तो हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को जगह देनी ही होगी. हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, पर अपने तरीके से. जब उस 90 प्रतिशत भारत को मौका मिलेगा अपनी बात कहने का तो वह हिन्दी में या अपनी भाषा में ही करेगा.
बहुतों ने इटली की एकता की 150वीं वर्षगाँठ पर भी लिखा है, चाहे यही लिखा हो कि वह देश की एकता नहीं मनाना चाहते, कि जीवन में और बहुत सी कठिनाइयाँ हैं नागरिकों की, वे लोग उनकी बात करना चाहते हैं, पर यह सब बातें इतालवी भाषा में लिख रहे हैं ...
अगर आज देश की एकता के लिए जान देने वाले लोग यहाँ आकर हमें देख सकते तो वे क्या सोचेंगे? वे हैरान होगें और खुश होंगे यह देख कर कि देश के उत्तर से ले कर दक्षिण तक कितने लोग इतालवी भाषा में लिख रहे हैं. उनके समय में यह देश विभिन्न बोलियों में बँटा था और उन्होंने निर्णय किया था कि देश को एक बनाने के लिए उसे एक भाषा देनी होगी. आज हम इस भाषा में कितना लिख रहे हैं, हर कोई किताब, कविता, चिट्ठा लिख रहा है, हम लिखते हुए थकते नहीं. इतालवी भाषा के विकिपीडिया में 7 लाख अस्सी हज़ार विषयों पर लेख हैं, इतने तो स्पेनी भाषा में भी नहीं जो कि बीस देशों में बोली जाती है. यह सच है इतालवी भाषा इन सालों में बहुत बिगड़ी है, पर जितनी जीवित आज है इतनी पहले कभी नहीं थी. आज हम सब इसी भाषा के गाने गाते हैं, इसी भाषा में फ़िल्म देखते हैं, इसी भाषा में चेट करते हैं, चिट्ठे लिखते हैं."
तकनीकी में, विज्ञान में, इतिहास और कला में, आज कहीं भी विश्वविद्यालय स्तर की शोध का काम अगर हिन्दी में किया जाये तो उसे वह सम्मान नहीं मिलता जो अंग्रेज़ी में किये जाने वाले काम को मिलता है. शायद इसलिए कि आज उस 90 प्रतिशत की आर्थिक ताकत कम है. लेकिन कल तकनीकी के विकास के साथ जब वह 90 प्रतिशत इन विषयों को समझना जानना चाहेगा, तो हिन्दी में यह काम बढ़ेगा, इसलिए नहीं कि कुछ लोग हिन्दी प्रेमी हैं, बल्कि इसलिए कि बाज़ार उसकी माँग कर रहा है.

जिन्हें हम भारत में "अंग्रेज़ी भाषी" कहते हैं, उनमें से बहुत सा हिस्सा बोलने लायक अंग्रेज़ी तो जानता है पर वह भारतीय अंग्रेज़ी है जिसे समझने के लिए विदेशियों को अनुवाद की आवश्यकता होती है. इस अध कच्ची अंग्रेज़ी का विकास किस ओर होगा? शुद्ध अंग्रेज़ी की ओर या अपनी भाषाओं की ओर? जब भारतीय भाषाओं का बाज़ार बढ़ेगा तो क्या यह भारतीय अंग्रेज़ी एक दिन उन्हीं में घुल मिल जायेगी?