बहुत साल पहले एक पत्रिका होती थी "सारिका", उसमें किशन चन्दर की एक कहानी छपी थी "नीले फीते का जहर". क्या था उस कहानी में यह याद नहीं, बस यही याद है कि कुछ ब्लू फ़िल्म की बात थी. पर दुकानों पर लटकती चमकीली थैलियों के फीते देख कर मुझे हमेशा उसके शीर्षक की याद आ जाती है.
हवा में लटकते फीते किसी बुद्ध मन्दिर में फहराते प्रार्थना के झँडों की तरह सुन्दर लगते हैं. इन थैलियों में शैम्पू, काफी, मक्खन, आदि विभिन्न चीज़ें बिकती हैं, जिनमें कोई जहर नहीं होता. इन झँडों में आम भारतीय उपभोगता की स्वाभाविक चालाकी की कहानी भी है जोकि बड़े बहुदेशीय कम्पनियों के बिक्री मैनेजरों को ठैंगा दिखाती है. तो फ़िर क्यों यह थैलियाँ हमारे जीवन में जहर घोल रही हैं?
थैलियों से जान पहचान
छोटी छोटी यह चमकीली थैलियाँ देखीं तो पहले भी थीं, लेकिन पहली बार उनके बारे में सोचा जब पिछले साल स्मिता के पास केसला (मध्य प्रदेश) में ठहरा था.
थैलियों को कूड़े में देख कर मैंने स्मिता की साथी शाँतीबाई से पूछा था, इस कूड़े का क्या करती हो? यह भी क्या सवाल हुआ, उसने अवश्य अपने मन में सोचा होगा, यहाँ क्या गाँव में कोई कूड़ा उठाने आता है? नींबू या फल सब्जी का छिलका हो तो रसोई के दरवाज़े से पीछे खेत में फैंक दो. और प्लास्टिक या एलूमिनियम की थैली हो तो जमा करके जला दो, और क्या करेंगे इस कूड़े का?
इसीलिए यह थैलियाँ दूर दूर के गाँवों की हवा में रंग बिरंगी तितलियों की तरह उड़ती हैं. लाखों, करोड़ों, अरबों थैलियाँ. भारत इन चमकीली थैलियों की दुनिया भर की राजधानी है.
एक ओर यह थैलियाँ भारत में अरबों रुपयों की बिक्री करने वाली कम्पनियों के लिए सिरदर्द बनी हैं. वह कम्पनियाँ भी कोशिश करके हार गयीं लेकिन इसका हल नहीं खोज पायीं कि कैसे थैलियों में बेचना कम किया जाये, ताकि मुनाफ़ा बढ़े. उनको हवा में तितलियों की तरह उड़ने वाली थैलियों की चिन्ता नहीं, उनको चिन्ता है कि इन थैलियों से छुटकारा पा कर कैसे अपनी कम्पनी के लाभ को अधिक बढ़ायें.
आज जब "स्वच्छ भारत" की बात हो रही है, तो इन थैलियों की कथा को समझना भी आवश्यक है.
थैंलियाँ कैसे आयीं भारत में?
छोटी थैलियों में चीज़ बेचना यह एक भारतीय दिमाग का आविष्कार था - श्री सी के रंगानाथन का.
तमिलनाडू के कुडालूर शहर के वासी श्री रंगानाथन ने 1983 में चिक इन्डिया (Chik India) नाम की कम्पनी बनायी, जो चिक शैम्पू बनाती थी. उन्होंने चिक शैम्पू को छोटी एलूमिनियम की थैलियों में बेचने का सोचा. उनका सोचना था कि गाँव तथा छोटे शहरों के लोग एक बार में शैम्पू की बड़ी बोतल नहीं खरीद सकते, लेकिन वह भी शैम्पू जैसी उपभोगत्ता वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं, तो कम दाम वाली एक रुपये की थैली खरीदना उनके लिए अधिक आसान होगा. उनकी सोच सही निकली और चिक इन्डिया को बड़ी व्यवसायिक सफलता मिली.
1990 में चिक इन्डिया का नाम बदल कर ब्यूटी कोस्मेटिक प्र. लि. रखा गया और 1998 इसके नाम का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ तथा यह "केविन केयर प्र. लि." (CavinKare Pvt. Ltd.) कर दिया गया. श्री रंगनाथन को कई पुरस्कार मिल चुके हैं तथा उन्होंने विकलाँग मानवों के साथ काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था "एबिलिटी फाउँनडेशन" भी स्थापित की है.
1991 में जब नरसिम्हाराव सरकार ने भारत के द्वार उदारीकरण की राह पर खोले तो दुनियाभर की बड़ी बड़ी बहुदेशीय कम्पनियों ने सोचा कि करोड़ों लोगों की आबादी वाले भारत के बाज़ार में उनकी कमाई के लिए जनता उनकी प्रतीक्षा में बैठी थी. इन कम्पनियों के कुछ उत्पादनों को FMCG (Fast Moving Consumer Goods) यानि "अधिक बिक्री होने वाली उपभोगत्ता वस्तुएँ" के नाम से जाना जाता है, छोटी थैलियाँ उन्हीं उत्पादनों से जुड़ी हैं.
इन कम्पनियों ने जोर शोर से भारत में अपने उद्योग लगाये और वितरण प्लेन बनाये, लेकिन जिस तरह की बिक्री की आशा ले कर यह कम्पनियाँ भारत आयी थीं, वह उन्हें नहीं मिली. कुछ ही वर्षों में लगातार घाटों के बाद सबमें हड़बड़ी सी मच गयी.
जब बहुदेशीय कम्पनियों को भारत के बाज़ार में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने भी छोटी थैलियों की राह पकड़ी. उनका सोचना था कि सस्ती थैलियों के माध्यम से एक बार लोगों को उनकी ब्रैंड की चीज़ खरीदने की आदत पड़ जायेगी तो वह बार बार दुकान में जा कर सामान खरीदने के बजाय उनकी बड़ी बोतल खरीदेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उनकी छोटी थैलियाँ खूब बिकने लगीं, लेकिन उनकी बड़ी बोतलों की बिक्री जितनी बढ़ने की उन्हें आशा थी, वैसा नहीं हुआ.

भारत में लोग हर चीज़ को माप तौल कर यह देखते हैं कि कहाँ अधिक फायदा है, और लोगों ने छोटी थैलियों के साथ भी यही किया. अगर आप बड़ी बोतल के बदले उतनी ही चीज़ छोटी पचास या सौ थैलियों में खरीदें तो आप को उसकी कीमत बोतल के मुकाबले कम पड़ती है. इसलिए अधिकतर लोग सालों साल तक छोटी थैलियाँ ही खरीदते रहते हैं, कभी बड़ी बोतल की ओर नहीं जाते. जैसा विदेशों में होता कि हफ्ते में एक दिन जा कर इकट्ठा सामान खरीद लो, वैसा भारत के छोटे शहरों व गावों में नहीं होता. अधिक सामान को खरीद कर कहाँ रखा जाये, यह परेशानी बन जाती है. लोग करीब की दुकान से हर दिन जितनी ज़रूरत हो उतना खरीदना बेहतर समझते हैं, और जिस दिन पैसे कम हों, उस दिन नहीं खरीदते. बड़ी बड़ी कम्पनियों को आखिरकार हार माननी पड़ी. अब उनसे न छोटी थैलियाँ का उत्पादन बन्द करते बनता है और जिस तरह की बिक्री की वह सोचती थीं वह भी उनके हाथ नहीं आयी.
आज छोटे गाँव हों या छोटे बड़े शहर, हर जगह आप को नुक्कड़ की दुकानों में भारतीय तथा बहुदेशीय कम्पनियों की यह छोटी थैलियाँ रंग बिरंगी चमकीली झालरों की तरह लटकी दिखेंगी. इन थैलियों को तकनीकी भाषा में सेशे (sachet) कहते हैं.
कैसे बनती हैं सेशे की छोटी थैलियाँ?
छोटी थैलियों को बनाने में एलुमिनियम, प्लास्टिक तथा सेलूलोज़ लगता है. इनमें एलूमिनियम की एक महीन परत को सेलूलोज़ की या प्लास्टिक की दो महीन परतों के बीच में रख कर उन्हें जोड़ा जाता है. यह बहुत हल्की होती है और इनके भीतर के खाद्य पदार्थ, चिप्स, नमकीन या शैम्पू आदि न खराब होते हैं, न आसानी से फटते हैं. इस तकनीक से थैलियों के अतिरक्त ट्यूब, डिब्बा आदि भी बनाये जाते हैं.
उपयोग के बाद, खाली थैलियों से, माइक्रोवेव की सहायता से एलूमिनियम तथा हाइड्रोकारबन गैस बनाये जा सकते हैं. एलुमिनियम विभिन्न उद्योगों में लग जाता है जबकि हाईड्रोकार्बन गैस उर्जा बनाने में काम आती है. लेकिन अगर इन्हें जलाया जाये तो उससे हानिकारक पदार्थ हवा में चले जाते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषित होता है.
एलूमिनयम की जानकारी सोलहवीं शताब्दी में आयी थी लेकिन इस धातू की वस्तुएँ बनाने में सफलता मिली सन् 1855 में. उस समय इसे "मिट्टी की चाँदी" कहते थे, क्योंकि तब यह बहुत मँहगी धातू थी और इससे केवल राजा महाराजाओं के प्याले-प्लेटें या गहने बनाये जाते थे.
एलुमिनियम को सस्ते या टिकाऊ तरीके से बनाने की विधि 1911 में खोजी गयी और धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ा और साथ ही इसकी कीमत गिरी. आज एलूमिनियम के बरतन अन्य धातुओं के बरतनों से अधिक सस्ते मिलते हैं और अक्सर गरीब घरों में प्रयोग किये जाते हैं. हर वर्ष दुनिया में लाखों टन एलूमिनयम का उत्पादन होता है जिन्हें बोक्साइट की खानों से निकाल कर बनाया जाता है. खानों की खुदाई से पर्यावरण तथा जनजातियों के जीवन की कुछ समस्याएँ जुड़ी हैं जैसा कि ओडिशा में वेदाँत कम्पनी की बोक्साइट की खानों के विरुद्ध जनजातियों के अभियान में देखा जा रहा है.
इस स्थिति में बजाय छोटी थैलियों को कूड़े की तरह फैंक कर पर्यावरण की समस्याएँ बढ़ाने से बेहतर होगा कि उन थैलियों के भीतर के एलूमिनियम को दोबारा प्रयोग के लिए निकाला जाये. इससे कूड़ा भी कम होगा. विकसित देशों में एलुमिनियम के पुनर्पयोग के कार्यक्रम आम है.
भारत में भी कुछ जगह एलुमिनयम के पुनर्पयोग के उदाहरण मिलते हैं लेकिन यह बहुत कम हैं. हमारे देश में अधिकतर जगह इन थैलियों में छुपी सम्पदा को नहीं पहचाना जाता, बल्कि उन्हें कूड़ा बना कर जलाया जाता है या जमीन में गाड़ा जाता है, जिससे नयी समस्याएँ बन जाती हैं.
गुवाहाटी का उदाहरण
यहाँ एक ओर तो जोर शोर से स्वच्छता अभियान की बात होती है, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि शहर में सफ़ाई रखिये. दूसरी ओर, हमारे शहरों में कूड़ा इक्ट्ठा करने का आयोजन ठीक से नहीं होता. गुवाहाटी (असम) में भी यही हाल है. शहर में कूड़े के डिब्बे खोजने लगेंगे तो खोजते ही रह जायेंगे. प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों या मन्दिरों के आस पास भी कूड़े के डिब्बे नहीं मिलते. खुली जगह पर पिकनिक हो, कोई विवाह समारोह या पार्टी हो, या मन्दिरों में त्योहार की भीड़, लोग आसपास कूड़े के ढ़ेर लगा कर छोड़ जाते हैं.
कूड़े के डिब्बों की जगह पर, शहर में कई कई किलोमीटर की दूरी पर बड़े कूड़ा एकत्रित करने वाले कन्टेनर मिलते हैं. यानि आप पिकनिक पर जायें या मन्दिर जायें, तो उसके बाद कूड़े के थैले ले कर इन कन्टेनरों को खोजिये. अक्सर लोग दूर रखे कम्टेनर तक जाने की बजाय कूड़े को वहीं फैंक देते हैं. पिकनिक स्थलों पर प्लास्टिक की थैलियाँ, चमकीली कागज़ की प्लेटें, मुर्गियों के पँख, इधर उधर उड़ते रहते हैं. (तस्वीर में गुवाहाटी के उमानन्द मन्दिर के पीछे फैंका हुआ कूड़ा)

गुवाहाटी में छोटी थैलियों का क्या किया जाता है, मैं यह समझना चाहता था. इसी की खोज में मैं एक दिन, शहर के करीब ही, हाईवे से जुड़े "बोड़ो गाँवो" गया, जहाँ ट्रकों से गुवाहाटी शहर का सारा कूड़ा जमा होता है. उस जगह पर, बहुत दूर से ही कूड़े की मीठी गँध गाँव के हवा में बादलों की तरह सुँघाई देती है. इस कूड़े से कई सौ परिवारों की रोज़ी रोटी चलती है. वह लोग झोपड़ियों में कूड़े के आसपास ही रहते हैं. झोपड़ियों के आसपास भी कूड़े के ढ़ेर लगे होते हैं जहाँ उसकी छटाई होती है और जो वस्तुएँ बेची जा सकती हैं, वह निकाल ली जाती हैं. वहाँ कोई विरला ही लिखना पढ़ना जानता है, तथा बच्चे भी स्कूल नहीं जाते.

आज की दुनिया में हमारे शहरों में व्यवसाय तथा लोग कूड़ा बनाने में माहिर हैं. हर दिन हमारे यहां लाखों टन कूड़ा बनता है. लेकिन सभी कूड़ा बनाने वाले, अपने कूड़े से और उसकी गन्ध से नफरत करते हैं. ऐसी स्थिति में शिव की तरह विष पीने वाले, कूड़े में रह कर काम करने वाले लोग जो उस कूड़े से पुनर्पयोग की वस्तुएँ निकालते हैं, उन्हें तो संतों का स्थान मिलना चाहिये. पर हमारा समाज उनके इस काम की सराहना नहीं करता बल्कि उन्हें समाज से क्या मिलता है, इसकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं.
उन कूड़े के ढेरों पर बहुत से पशु पक्षी भी घूमते दिखते हैं, जिनमें असम के प्रसिद्ध ग्रेटर एडजूटैंट पक्षी भी हैं.
कूड़े में अधिकतर स्त्रियाँ तथा बच्चे काम करते हैं. कई बच्चे तीन चार साल के भी दिखे, जो कूड़े की थैलियाँ सिर पर उठा कर ले जा रहे थे. जब भी नगरपालिका का कोई ट्रक आता, वह लोग उसके पीछे भागते ताकि कूड़े को चुनने का उन्हें पहले अवसर मिले.
कूड़े में काम करने वालों का क्या जीवन है, उनकी समस्याएँ क्या है, यह जानने नहीं गया था. उसके बारे में फ़िर कभी लिखूँगा. बल्कि मेरा ध्येय था यह जानना कि खाली थैलियों का क्या होता है?
संयोग से, वहाँ पहुँचते ही एक टेम्पो दिखा जिस पर कई हज़ार खाली थैलियाँ प्लास्टिक में बँधी थीं. मैंने उस टेम्पो को देख कर सोचा कि इसका अर्थ था कि खाली थैलियों को अलग कर के रखा जाता है, यानि इन्हे बेचने का तथा इनके पुनर्पयोग का कुछ कार्यक्रम चल रहा है.
पर ऐसा नहीं था. थोड़ी देर बाद वह टेम्पो भी कूड़े के ढेर की ओर बढ़ा जहाँ अन्य ट्रक अपना कूड़ा फैंक रहे थे. टेम्पो वाले युवकों ने प्लास्टिक को खोल कर उन खाली थैलियों को अन्य कूड़े के बीच में फैंक दिया.
स्वच्छ भारत
जब तक शहरों में कूड़ा फैंकने की उपयुक्त जगहें नहीं होंगी, लोगों को यह कहने का क्या फायदा है कि सफाई रखिये? शहरों में जगह जगह पर डिब्बे होना जिसमें लोग कूड़ा डाल सके, आवश्यक हैं. मन्दिर तथा पिकनिक स्थलों पर भी कूड़ा जमा करने के डिब्बे रखना ज़रूरी है.
हम से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहे कि वह स्वच्छ भारत नहीं चाहता. लेकिन क्या सड़कों पर झाड़ू लगाने या डिब्बों में कूड़ा फैंकने से भारत स्वच्छ हो जायेगा? झाड़ू लगा कर कूड़ा हटाना तथा डिब्बों में कूड़ा डालना तो केवल पहला कदम है. इससे शहरों में रहने वाले लोगों के सामने की गन्दगी हटती है. लेकिन वही गन्दगी हमारे शहरों के बाहर अगर जमा होती रहती है, तो क्या सच में हमारा वातावरण स्वच्छ हो गया?
देश में हर दिन लाखों करोड़ों टन नया कूड़ा बनता है, उसका क्या करेंगे हम? उसे जला कर वातावरण का प्रदूषण करेंगे या जितना हो सकेगा उसका पुनर्पयोग होना चाहिये?
चमकीली थैलियों में छुपे लाखों टन एलूमिनियम को निकाल कर उसका दोबारा उपयोग करना बेहतर है या नयी खानें बनाना?
फल सब्जी आदि खाद्य पदार्थों के कूड़े को जमा करके उनसे खाद बनाने से बेरोजगार लोगों को जीवनयापन के माध्यम मिल सकते हैं. वैसे ही थैलियों में छुपे एलुमिनियम के पुनर्पयोग से भी उद्योगों तथा बेरोजगार युवकों को फायदा हो सकता है. बोड़ा गाँव जैसी जगहों में कूड़ा जमा करने वाले लोगों को भी इससे जीवनयापन का एक अन्य सहारा मिलेगा. साथ ही कूड़ा जलाने से जो प्रदुषण होता है वह कम होगा.
जब तक ऐसे प्रश्नों के बारे में नहीं सोचेगें, भारत स्वच्छ हो, यह सपना सपना ही रहेगा और चमकीली थैलियाँ समृद्धी का रास्ता बनने के बजाय, जहर बन कर किसी शिव की प्रतीक्षा करती रहेंगी.
***

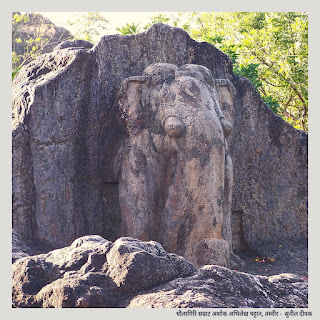


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
01.jpg)




















